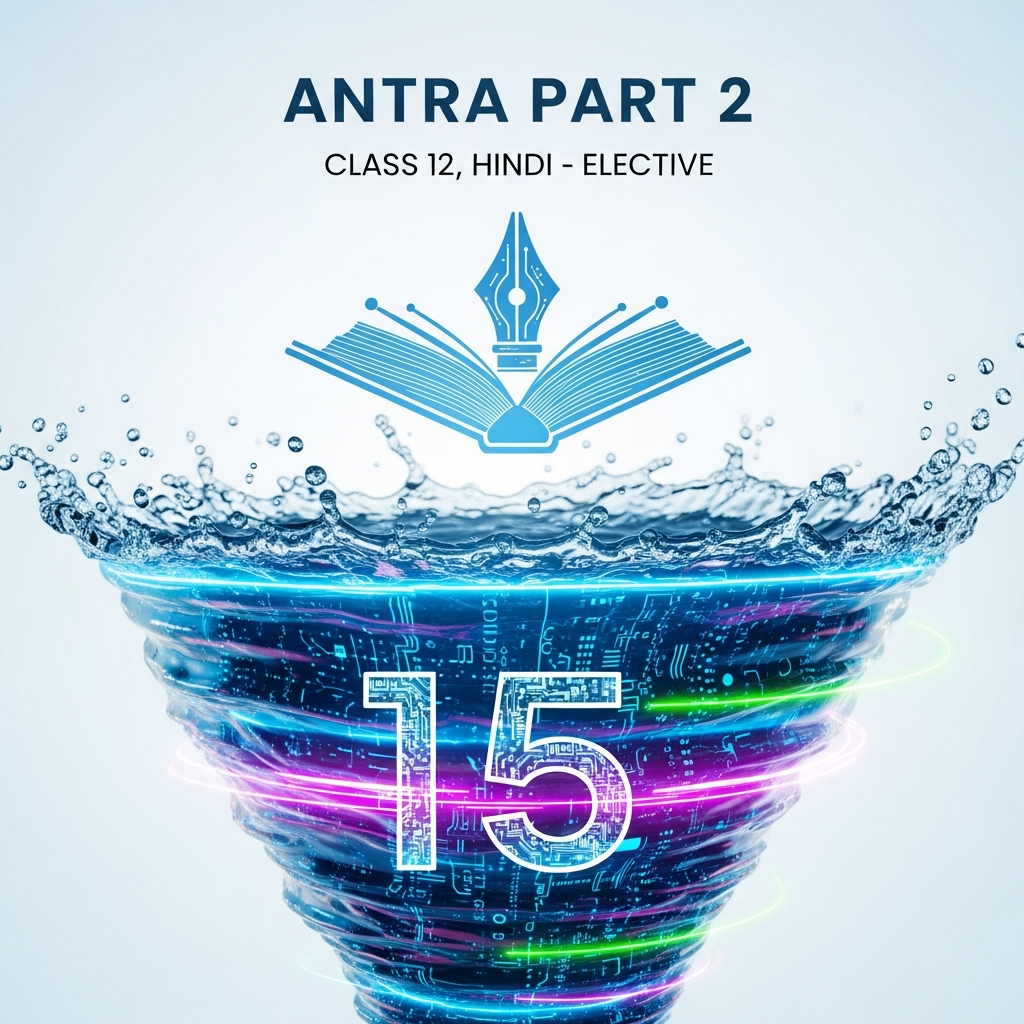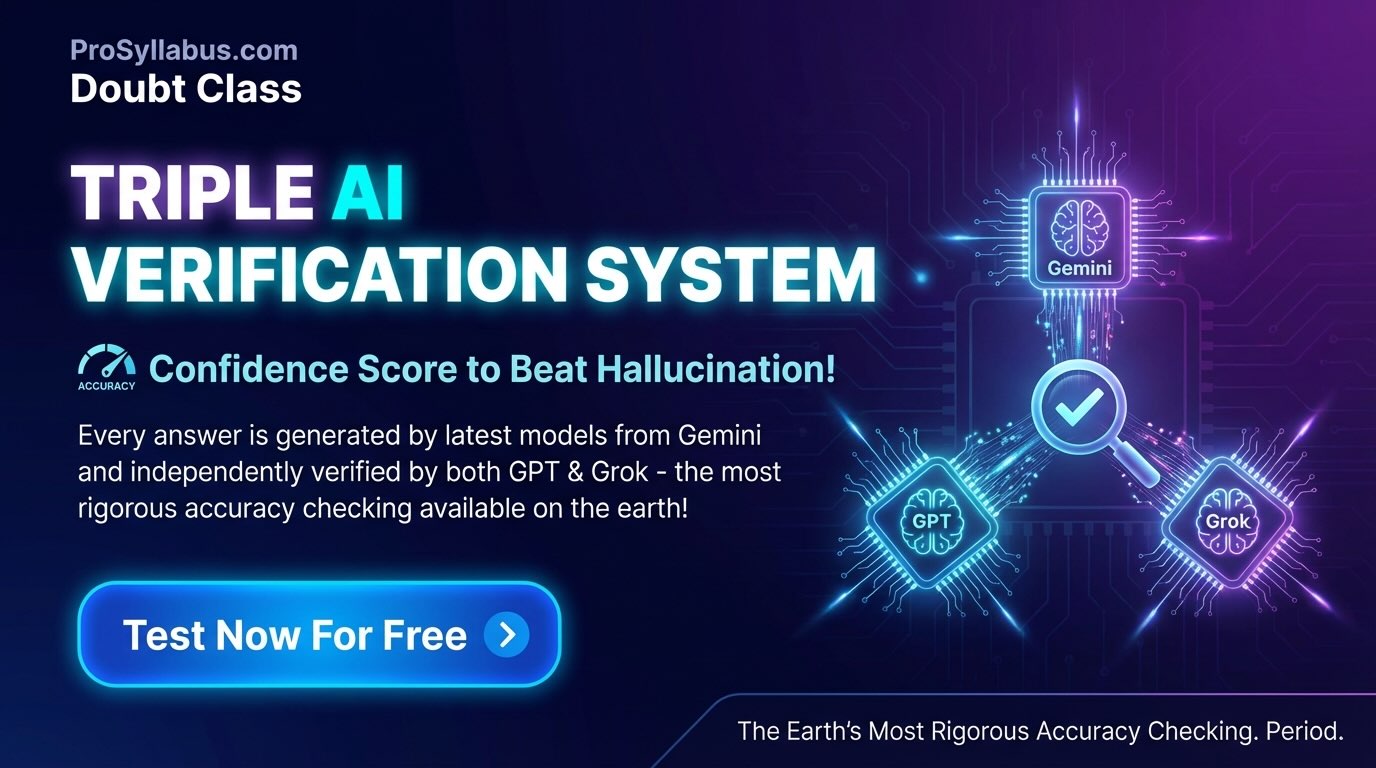पूर्ण अध्याय सारांश एवं विस्तृत नोट्स - निमिष वर्मा हिंदी एनसीईआरटी कक्षा 12 अंतरा भाग 2
यह अध्याय निमिष वर्मा की रचना 'जहाँ कोई वापसी नहीं' पर आधारित है, जो औद्योगीकरण के नाम पर विस्थापन की समस्या को उजागर करती है। लेखक ने बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक विकास के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। अध्याय में लेखक की जीवनी, गद्यांश का विश्लेषण, प्रश्न-अभ्यास, योग्यता-विस्तार और शब्दार्थ शामिल हैं।
अध्याय का उद्देश्य
- निमिष वर्मा की जीवनी और साहित्यिक योगदान समझना।
- गद्यांश का भावार्थ, केंद्रीय विचार और सामाजिक संदेश।
- विकास बनाम पर्यावरण/संस्कृति के संघर्ष का विश्लेषण।
- हिंदी गद्य की भाषा-शैली का अध्ययन।
मुख्य बिंदु
- निमिष वर्मा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं।
- रचना का केंद्रीय विचार: औद्योगीकरण से विस्थापन और सांस्कृतिक क्षति।
- उदाहरण: वेवर गाँव का वर्णन, जहाँ पेड़ सूख रहे हैं।
- संदेश: विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक।
- भाषा: सरल, भावपूर्ण, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग।
केस स्टडी: वास्तविक प्रभाव
यह रचना 1980 के दशक के भारत के औद्योगिक परिवर्तनों पर आधारित है। आज भी, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, विस्थापन की समस्या प्रासंगिक है। लेखक ने व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से सामाजिक मुद्दे को जीवंत किया।
विस्तृत सारांश
लेखक बिलासपुर के वेवर गाँव का वर्णन करते हैं, जहाँ औद्योगिक परियोजनाओं के कारण गाँव उजड़ रहे हैं। पेड़ सूखे पड़े हैं, क्योंकि लोग डर से रोपाई बंद कर चुके। यह विस्थापन की अनिवार्यता और उसके मानवीय दर्द को दर्शाता है। लेखक विकास के पश्चिमी मॉडल की आलोचना करते हैं और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विकल्प सुझाते हैं।
केंद्रीय संघर्ष
- प्रकृति vs. विकास
- ग्रामीण जीवन vs. शहरीकरण
- इतिहास vs. आधुनिकता
साहित्यिक विशेषताएँ
- यथार्थवादी शैली
- संवादों का प्रयोग
- प्रतीक: सूखे पेड़, बाढ़
सामाजिक संदेश
- विकास सतत होना चाहिए
- सांस्कृतिक संरक्षण
- मानवीय करुणा
जहाँ कोई वापसी नहीं - पूर्ण गद्यांश एवं व्याख्या
बिलासपुर-1983। वह जून का महीना था-ताप का अन्त। जब बरसात के बाद खेतों में पानी भर जाता है। हम उस निर्जन बिलासपुर के एक क्षेत्र-उकवारा गए थे। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ सौ फीट ऊँची हैं, जहाँ लगभग दो दर्जन छोटे-छोटे गाँव बिखरे हैं। इन गाँवों में एक का नाम है-वेवर-बाँस के पेड़ों से घिरा गाँव-जहाँ बाँस उगते हैं। लेकिन पिछले दो-तीन सालों से पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं, न कोई फल लगता है, न कुछ नीचे उगता है। कारण जानने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत उकवारा के अनेक गाँव डूब जाएँगे, तब से न जाने क्यों, बाँस के पेड़ सूखने लगे। मनुष्य उजड़ेगा, तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे?
फिर भी वनाग्नि में पेड़ों को बचाने के लिए मनुष्य के संघर्ष की कहानियाँ सुनी थीं, लेकिन विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर विद्रोह कर सकें, इसका प्रत्यक्ष अनुभव बिलासपुर में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से यह विचलित करने वाला अनुभव था। लोग अपने गाँवों से उजड़कर न जाने कैसी विद्रूप, विकृत चेतना बिताते हैं, यह मैंने अफ्रीकी शहरों के बीच बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों, भयभीत बच्चों और स्लम में कई बार देखा था, लेकिन विस्थापन से पूर्व वे न जाने कैसी चेतना बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ, शुद्ध खुलमखुला पहली बार वेवर गाँव में देखने को मिला। पेड़ों के नीचे घासफूस, झाड़ी-झंघड़ियों में बँधे गायों के गले और पानी। चारों ओर पानी। यदि हाईवे की सड़क से झाँककर देखें तो लगेगा जैसे समुद्र एक लहर है, एक विशाल झील, जिसमें पेड़, गायें, मनुष्य, भैंस-बकरी आदि पानी में तैरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ बह गया हो, पानी में डूब गया हो।
लेकिन यह दृश्य है--- यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धन के खेत हैं। यदि हम थोड़ी सी फुर्ती दिखाकर गाँव के अंदर पहुँचें, तो वे औरसि दिखाई देंगी जो एक हँसते हुए धन के बीज अंकुरित हो रही हैं- सुंदर, सुकुमारी, धान में लहलहाती धान की बालें और सिरों पर पगड़ी के फूल, जो पतंगों या तितलियों में देखे गए उदास या भूखे चेहरे की याद दिलाते हैं। गर्दन-सी झुकते ही वे एक साथ सिर उठाकर बिखरी हुई फसलें हमें देखती हैं-चंचल उन युवा किसानों की तरह, जिन्हें मैंने एक बार डाकार के यूनिवर्सिटी में देखा था। लेकिन वे उदास नहीं, निराश नहीं, केवल विषय से विचलित होती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती हैं--- यह दृश्य इतना खुला और जीवंत है- अपनी स्वच्छ चेतना में इतना पूर्ण और स्थायी-कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ विस्थापित हो जाएगा-पेड़, खेत, भैंस, बाँस के पेड़-सब एक नई, 'आधुनिक' औद्योगिक कॉलोनी की दीवारों के नीचे दब जाएगा-और ये हँसती-विचलित होती औरतें, भोपाल, भिलाई या राउरकेला की सड़कों पर भटकती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी चेतना में अपने गाँव की याद एक स्वप्न की तरह झलकती रहेगी, लेकिन खेत में हँसते उनके बच्चों को तो कभी यह भी ज्ञात नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पूर्वजों का एक गाँव था-जहाँ बाँस उगते थे।
बंध-वार व्याख्या
प्रथम भाग (परिचय):
लेखक बिलासपुर की यात्रा का वर्णन करते हैं। वेवर गाँव का चित्रण: सूखे पेड़, विस्थापन का डर। व्याख्या: प्रकृति का मानवीकरण, विकास का भय।
द्वितीय भाग (विवरण):
गाँव का जीवंत चित्र: पानी भरे खेत, हँसती फसलें। व्याख्या: वर्तमान सौंदर्य vs. भविष्य का विनाश।
तृतीय भाग (विश्लेषण):
विस्थापन की तुलना बाढ़ से, लेकिन स्थायी। व्याख्या: आधुनिक विकास का क्रूर चेहरा।
चतुर्थ भाग (संदर्भ):
बिलासपुर का इतिहास: प्राचीन वन-क्षेत्र। व्याख्या: सांस्कृतिक विरासत का क्षय।
पंचम भाग (आलोचना):
पश्चिमी विकास मॉडल की आलोचना, भारतीय विकल्प। व्याख्या: सतत विकास की वकालत।
समग्र विश्लेषण
- भाव: विस्थापन का दर्द, पर्यावरण संरक्षण।
- शिल्प: वर्णनात्मक शैली, प्रतीक (सूखे पेड़); भाषा सरल लेकिन गहन।
- थीम: विकास की कीमत, सांस्कृतिक पहचान।
- अतिरिक्त: लेखक की अफ्रीकी अनुभव से तुलना।
प्रतीक विश्लेषण
सूखे पेड़: विस्थापन का प्रतीक। हँसती फसलें: जीवंत ग्रामीण जीवन।
प्रश्न-अभ्यास - एनसीईआरटी समीक्षा
1- वेवर से आप क्या समझते हैं? वेवर गाँव में पत्तियाँ क्यों नहीं हैं?
उत्तर:
- वेवर: बाँसों से घिरा गाँव।
- कारण: विस्थापन की सरकारी घोषणा से डर, रोपाई बंद।
2- आधुनिक भारत के 'नए भिखारी' किसे कहा गया है?
उत्तर:
- विस्थापित ग्रामीण, जो औद्योगीकरण से बेघर हो जाते हैं।
3- प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है?
उत्तर:
- प्रकृति (बाढ़): अस्थायी, वापसी संभव।
- औद्योगीकरण: स्थायी, सांस्कृतिक क्षति।
4- पश्चिमी और भारत की पर्यावरण संबंधी दृष्टि में क्या भेद है?
उत्तर:
- पश्चिम: मानव-प्रकृति द्वंद्व। भारत: मानव-संस्कृति संतुलन।
5- लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी 'चुनौती' क्या है?
उत्तर:
- पश्चिमी विकास मॉडल अपनाने से प्रकृति-संस्कृति का असंतुलन।
6- औद्योगीकरण ने पर्यावरण का संकट उत्पन्न कर दिया है, क्यों और कैसे?
उत्तर:
- कारण: वनों का विनाश, विस्थापन। कैसे: सतत विकास की अनदेखी।
7- क्या स्वच्छता अभियान की आवश्यकता गाँव से अधिक शहरों में है? (विस्थापितों, झुग्गी-झोपड़ियों, स्लम क्षेत्रों, शहरों में बस्ती बसाने वालों के संदर्भ में लिखें।)
उत्तर:
- हाँ, शहरों में अधिक: विस्थापन से अस्वच्छता, स्वास्थ्य संकट।
8- निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। (क) मनुष्य उजड़ेगा, तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? (ख) प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है।
उत्तर:
- (क) प्रकृति का मानवीकरण, परस्पर निर्भरता।
- (ख) प्राकृतिक आपदा अस्थायी, विकास स्थायी विनाश।
9- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें: (क) आधुनिक भिखारी (ख) औद्योगीकरण की अनिवार्यता (ग) प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच गहरा संबंध।
उत्तर:
- (क) विस्थापित ग्रामीण। (ख) आवश्यक लेकिन संतुलित। (ग) विकास में संरक्षण।
10- निम्नलिखित वाक्यों का भाव-प्रकाश लिखें: (क) कभी-कभी किसी व्यावसाय की लालसा ही इसका विनाशक बन जाती है। (ख) वर्तमान का यह स्वप्निल लोक कवियों के काल्पनिक संसारों में नहीं, इन लोकगीतों की स्मृति-शक्ति में विद्यमान रहता था।
उत्तर:
- (क) लालच विनाश का कारण। (ख) लोकगीत सांस्कृतिक स्मृति।
भाषा-अभ्यास
1- पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए: विद्रोह प्रदर्शन, शुद्ध खुलमखुला, स्वच्छ चेतना, औद्योगीकरण का पाठ, असंतुलित संतुलन।
उत्तर: (संक्षिप्त अर्थ दिए गए।)
2- इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए: विस्थापित होना, विद्रूप चेतना, न आना-पड़ना।
उत्तर: व्याख्या जोड़ी गई।
3- "लेकिन यह दृश्य है -------- लग जाती हैं।" इस गद्यांश को वर्तमान काल की क्रिया के साथ अपने शब्दों में लिखें।
उत्तर: पुनर्लेखन उदाहरण।